सेकुलरिज्म और संविधान (Secularism and Constitution)
भारतीय संविधान सेक्युलर ( Secular, भारतीय अनुवाद ‘पंथ-निरपेक्ष’) है या नहीं ? यह प्रश्न सार्वजनिक विमर्श का विषय रहा है। भारतीय संविधान के सेक्युलर होने अथवा न होने, दोनों ही पक्षों में तर्क प्रस्तुत किये जाते रहे है और जाते रहेंगे।
लेखक : मृत्युञ्जय
सेक्युलरिज्म वास्तव में जितनी दिखती है उतनी सरल अवधारणा नहीं है। मोटे तौर पर उसका अर्थ राज्य और पंथ (religion) के पृथक्करण से है। यह अवधारणा मध्ययुगीन यूरोप में चर्च के राजनैतिक अधिकारों में कटौती करने के एक उपकरण के रूप में अस्तित्व में आयी। मध्ययुग में ईसाई सांप्रदायिक मठों को असीमित राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे या यूँ कहें कि उन्होंने ये अधिकार अपने धार्मिक एकाधिकार के फलस्वरूप प्राप्त कर लिए थे। चर्च द्वारा उपभोग किये जा रहे इन असीमित राजनैतिक अधिकारों को नियंत्रण में लाने के लिए सेक्युलरिज्म की इस अवधारणा का आविष्कार किया गया। एक नए सामाजिक-राजनैतिक मानक के रूप में यह अवधारणा अपने निर्धारित लक्ष्य, अर्थात चर्च के राजनैतिक अधिकारों में कटौती के लक्ष्य, को प्राप्त करने में पर्याप्त मात्रा में सफल भी रही। इसी सफलता के चलते आधुनिक युग में किसी भी राजनैतिक व्यवस्था में सेक्युलरिज्म के अस्तित्व को धार्मिक निष्पक्षता के उच्च मानक के रूप में सार्वत्रिक रूप में स्वीकार किया जाने लगा।
यूरोपीय रोग का एक टीका खोजा गया था और उसे सभी समाजों को लगाने का निश्चय किया गया, चाहे उन्हें वह रोग हो या न हो। यही टीका भारतीय राजनैतिक व्यवस्था को भी लगाया गया, बिना इस पैथोलोजिकल निर्धारण के कि क्या ‘सांप्रदायिक-मठों-को-असीमित-राजनैतिक-अधिकार’ नामक रोग के भारत की राजनैतिक व्यवस्था में कोई ऐतिहासिक लक्षण हैं अथवा भविष्य में इस प्रकार के लक्षण पनपने की कोई सम्भावना है?
किन्तु यदि सूक्ष्म रूप में देखें तो सेक्युलरिज्म एक अद्भुत अवधारणा है, जो भारत के समाज में प्रदीर्घ काल से फलती फूलती रही है। भले ही यूरोप को इसका ज्ञान अपने रोग के अंतिम चरण में पहुँचने के बाद हुआ हो, भारत में यह अवधारणा इतनी व्यापक रही कि इसे कभी कोई विशेष पारिभाषिक नाम देने की आवश्यकता ही नहीं जान पड़ी। अपने ‘सर्व-पंथ-समभाव’ के अन्तर्निहित गुण के कारण कभी किसी एक सम्प्रदाय को दीर्घकालीन असीमित राजनैतिक विशेषाधिकार प्राप्त ही नहीं हुये और यदि ऐसा होने की आशङ्का कभी हुई भी तो उसका निराकरण राजनैतिक स्तर पर न होकर धार्मिक स्तर पर ही किया गया। इस नाते पंथिक मामलों में राजनैतिक हस्तक्षेप और राजनैतिक मामलों में पंथिक हस्तक्षेप अत्यल्प ही देखने को मिलते हैं।
अब्राहमिक सम्प्रदायों में एकाधिकार की प्रवृत्ति है, जिससे राजनैतिक महत्वाकांक्षा पनपती है। स्वाभाविक रूप से ऐसी सांप्रदायिक-राजनैतिक व्यवस्था में अन्य पंथों के अस्तित्व के लिए सेक्युलरिज्म की नितांत आवश्यकता है किन्तु भारतीय सम्प्रदायों और पंथों में इस एकाधिकार की प्रवृत्ति और उससे पनपने वाली राजनैतिक महत्वाकांक्षा के सामान्यतः अभाव के होते हुये भी सेक्युलरिज्म की अवधारणा को पाश्चात्य सन्दर्भ में भारतीय राजनीति में अनावश्यक रूप से ठूँसा गया।
वर्तमान भारतीय राजनीति में सेक्युलर शब्द, भारतीय धार्मिक परम्पराओं के विरुद्ध, उन्हीं अब्राहमिक सम्प्रदायों के हाथ का अस्त्र बन गया है जिनसे निबटने के लिए इस शब्द और उससे जुड़ी अवधारणा का आविष्कार किया गया था। भारतीय धार्मिक परम्पराओं के विरुद्ध राजनैतिक हथियार के रूप में इस शब्द का व्यापक प्रयोग हालाँकि अधिक पुराना नहीं है।

भारतीय संविधान सभा की मुहर, Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.
वस्तुतः इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि मूल भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द का प्रयोग केवल एक स्थान पर हुआ था और वह भी सेक्युलर शब्द के वर्तमान अर्थ से एकदम विपरीत अर्थों में। अनुच्छेद 25 का उपबंध 2(a) संघ को नागरिकों की पंथिक या साम्प्रदायिक परम्पराओं से जुडी सेक्युलर गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, अर्थात मूल संविधान में प्रयुक्त सेक्युलर शब्द अजान जैसी धार्मिक परंपरा में, लाउडस्पीकर के उपयोग जैसी सेकुलर गतिविधि पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार सरकार को देता है जो सेक्युलर शब्द के वर्तमान प्रचलित अभिप्राय से बिलकुल विपरीत है।
वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द है, वह प्रक्षिप्त है और इसे 1977 में आपातकाल में किये गए 42 वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। सामान्यतः संविधान संशोधन मूल संविधान में सीमित परिवर्तन के लिए ही लाये जाते रहे है, किन्तु 42 वाँ संविधान संशोधन इतना व्यापक था कि कभी कभी इसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। संसद द्वारा संशोधन के माध्यम से जोड़े गए इस सेक्युलर शब्द की वैधानिकता निश्चित ही असंदिग्ध है, किन्तु संविधान की मूल प्रस्तावना में इस शब्द के अभाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान के वर्तमान स्वरुप में इस शब्द के अर्थपूर्ण अस्तित्व का हम इस आलेख के माध्यम से आकलन करने का प्रयास करेंगे।

अक्षर अङ्कन: प्रेम बिहारी नरायन रायज़ादा; चित्रकारी: बेवहर राममनोहर सिन्हा, सन् 1948-49 This work is in the public domain in India because its term of copyright has expired.
हमारे सामने दो प्रश्न उपस्थित होते हैं:
- सेक्युलर शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में क्यों नहीं था?
- क्या संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द के जोड़े जाने मात्र से संविधान या भारतीय राज्य सेक्युलर हो गया?
प्रथम प्रश्न के उत्तर को संविधान निर्माण की प्रक्रिया में खोजा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सेक्युलर शब्द को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम 42 वें संविधान संशोधन के दौरान ही आया। इसके पूर्व भी यह विचार संविधान निर्माताओ के मन में आया था और वस्तुतः संविधान के प्रारूप पर चर्चा के समय संविधान सभा में यह विचार प्रस्तुत भी किया गया था। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर बहस के दौरान प्रोफ़ेसर के. टी. शाह[1] ने संविधान के स्वरुप को स्थायी रूप से निर्धारित करने के लिए उसमें ‘सेक्युलर, फेडरल और सोशलिस्ट’ इन तीन शब्दों को जोड़े जाने का संशोधन प्रस्ताव रखा था। प्रोफेसर शाह ने कहा, “हर मंच से यह बार बार कहा जाता रहा है कि हमारा राज्य एक सेक्युलर राज्य है, यदि यह सत्य है तो मुझे इस शब्द को संविधान में न जोड़े जाने का कोई कारण नहीं दृष्टिगोचर होता।”
किन्तु इस संशोधन पर चर्चा के दौरान, इन शब्दों को जोड़े जाने के विरोध में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, “मुझे दुःख है कि मैं प्रोफ़ेसर के. टी. शाह के इन संशोधनों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूँ।” और अपनी बात पक्ष में उन्होंने तर्क दिया कि किसी एक समय का लोगों के जीने का ढंग आने वाले समय के लोगों के जीने के ढंग से भिन्न हो सकता है और इस प्रकार के शब्दों को स्थायी रूप से संविधान में जोड़ना आने वाले समय के लोगों के जीवन जीने के ढंग चुनने की स्वतंत्रता पर प्रहार होगा। उन्होंने आगे कहा,“मैं इस बात को उचित नहीं समझता कि संविधान लोगों को एक विशेष जीवन पद्धति से बाँध दे और लोगों को इस बात की स्वतंत्रता न दे कि आने वाले समय में वे अपनी जीवन पद्धति स्वयं चुन सके, और इसी एक कारण से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।”
बाद में संविधान सभा ने बहुमत से सेक्युलर सहित अन्य दोनों शब्दों को संविधान में जोड़ने वाला संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस एक बहस से यह एक बात तो स्पष्ट है कि भारत के संविधान निर्माताओं के मन में संविधान में सेक्युलर शब्द के प्रयोग को लेकर क्या विचार थे। यहाँ इस बात को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि न केवल संविधान निर्मात्री सभा का बहुमत, वरन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर भी इस ‘सेक्युलर’ शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़े जाने के पक्ष में नहीं थे।
दूसरा प्रश्न यह कि क्या संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द के जोड़े जाने मात्र से भारत एक ‘सेक्युलर’ राज्य बन गया?, यह प्रश्न संविधान के स्वरुप व संगठन से सम्बंधित है और संविधान के अन्य अनुच्छेदों के आलोक में हम इस बात की जाँच कर सकते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और इस अनुच्छेद में इंगित यह अधिकार किसी विशेष पंथ के लोगों के लिये सीमित न होकर, गणराज्य के सभी व्यक्तियों के लिए है। इन अर्थों में यह एक सेक्युलर प्रकार का अधिकार है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के इस अधिकार को उसके पंथ या सम्प्रदाय के आधार पर सीमित अथवा विस्तृत नहीं करता। इसी प्रकार संविधान में अन्य अनेक अधिकार और प्रावधान भी सेक्युलर हैं अर्थात नागरिक के पंथ से निरपेक्ष ये प्रावधान सभी नागरिकों पर सामान रूप से लागू हैं।
किन्तु सेक्युलर होने की कसौटी बहुत कठोर है, क्योंकि यदि राज्य-नीति-निर्धारक ग्रन्थ का कोई एक भी प्रावधान इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो संविधान की प्रस्तावना में प्रक्षिप्त इस शब्द की प्रतिबद्धता संदिग्ध हो जाती है, और प्रारूप समिति की अल्पसंख्यक उपसमिति की अनुसंशाओं के आधार पर जोड़े गए कुछ उपबंध, जो व्यक्ति के पंथ या सम्प्रदाय के आधार पर उसके कुछ अधिकारों को विनियमित करते हैं, संभवतः इसी श्रेणी में आते हैं।
जैसे, अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की, और निज पंथ को निर्बाधित रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। किन्तु, इसी अनुच्छेद का 2(b) हिन्दुओं के सन्दर्भ में इस अधिकार को सीमित करते हुए राज्य को यह अधिकार देता है कि हिन्दुओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को सभी के लिए खोलने, सामाजिक सुधार और समाज कल्याण के उद्देश्य से, सरकार अनुच्छेद 25 में प्रदत्त ‘पंथ को मानने, आचरण करने और प्रचार करने’ की इस स्वतन्त्रता को बाधित कर सकती है।
यहाँ उल्लेखनीय है कि हिंदू शब्द की इस परिभाषा में सिख, जैन और बौद्ध भी सम्मिलित हैं। अब यदि दूसरे शब्दों में कहें, तो यदि सरकार चाहे तो हिन्दुओं (सिख, जैन और बौद्ध सहित) की पंथिक स्वतंत्रता को, सामाजिक सुधार और समाज कल्याण के उद्देश्य से बाधित कर सकती है, (दही हांड़ी, जल्लीकट्टू, शनि मंदिर के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार मूलरूप से इसी उपबंध से आता है) । किन्तु ‘मुस्लिम और ईसाई पंथों में सामाजिक सुधार और समाज कल्याण के उद्देश्य से सरकार उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता को बाधित कर सकती है’, ऐसा कहने वाला कोई उपबंध नहीं है। अर्थात, यदि ईसाई अथवा मुस्लिम समाज यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि उनकी कोई प्रथा उनके पंथ के मूल ढाँचे से सम्बंधित है तो उस प्रथा को नियंत्रित करने वाला कोई भी सरकारी कानून, भले ही वह सामाजिक सुधार और समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया हो, स्वयमेव असंवैधानिक हो जायेगा (तीन तलाक, हिजाब, बहुविवाह से सम्बंधित कानून बनाने में हिचकिचाहट को इस परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है)।
यहाँ एक बात का उल्लेख करने का लोभ संवरण कर पाना कठिन है कि अनुच्छेद 25 में उल्लिखित शब्द “प्रचार” (propagation of religion) भी वस्तुत: अब्राहमिक पंथों के प्रभाव का ही परिणाम है, जैसा कि संविधान सभा में बहस के दौरान श्री पुरुषोत्तम दास टंडन[2] ने कहा था कि “I know that most Congressmen are opposed to this idea of “propagation”. But we agreed to keep the word “propagate” out of regard for our Christian friends.” यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि यद्यपि धर्म के प्रचार का यह अधिकार सभी पंथों के लिए समान रूप से उपलब्ध है किन्तु इसकी उपयोगिता हिन्दू, पारसी इत्यादि के लिए शून्य ही है।
इसी प्रकार, अनुच्छेद 30(1) देश के अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण बहुसंख्यक हिन्दू धर्म को प्राप्त नहीं है। इस अनुच्छेद के कारण हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य पंथों के व्यक्तियों के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओ में सरकारी हस्तक्षेप लगभग असंभव है। यही कारण है कि ईसाई और मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत लाने का सरकारी प्रयास विफल रहा और अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा नियंत्रित और संचालित शिक्षण संस्थायें इस कानून के अंतर्गत अपनी 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित करने के लिए बाध्य नहीं है[3]। उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अपनी कुल सीटों का 25 प्रतिशत इन वर्गों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है, शिक्षा के अधिकार के कानून का यह प्रावधान हिन्दू संचालित शिक्षण संस्थाओं पर, अल्पसंख्यक संस्थाओं की तुलना में एक प्रकार की आर्थिक निर्योग्यता लाद देता है।
संभवतः अनुच्छेद 30(1) के पंथ आधारित प्रावधानों के परिणामस्वरूप ही रामकृष्ण मिशन[4] द्वारा संचालित हिन्दू शिक्षण संस्थाओं ने स्वयं को हिन्दू से अलग अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने का प्रयास किया। जिस अनुच्छेद के द्वारा पोषित तुलनात्मक निर्योग्यताओं से बचने के लिए किसी हिंदू संस्था को तकनीकी रूप से अपना धर्म त्याग करने का मार्ग अवलंबन करना पड़े, क्या वह अनुच्छेद सेक्युलर है? और क्या ऐसे अनुच्छेद से युक्त संविधान वाला देश, सेक्युलर शब्द को प्रस्तावना में जोड़ मात्र देने से सेक्युलर हो जायेगा? इसी प्रतिप्रश्न के उत्तर में हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर निहित है।
धार्मिक आयाम में, विशेषकर हिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में, संविधान की स्थिति को समझने के लिए 3 और 6 दिसंबर 1948 की बहस के दौरान श्री लोकनाथ मिश्रा के भाषण[5] का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 दिसंबर को अपने भाषण का आरंभ करते हुए श्री लोकनाथ मिश्रा ने कहा कि, “मेरे विचार से संविधान के प्रारूप का अनुच्छेद 13[6] यदि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है तो अनुच्छेद 19[7] हिन्दुओं के लिए दासता का घोषणापत्र है, मैं वास्तव में इस बात का अनुभव करता हूँ कि यह सबसे अपमानकारक अनुच्छेद है और प्रारूप संविधान का सबसे स्याह हिस्सा है।”
6 दिसंबर को अपनी बात आगे रखते हुए श्री लोकनाथ मिश्रा ने कहा कि आरंभ में मैंने सोचा कि भारत का सेक्युलरिज्म दरअसल विभाजन के बाद बचे हिंदुबहुल क्षेत्र की उस क्षेत्र की अहिंदू जनता को एक उदार देन है किन्तु अब मुझे लगने लगा है कि यह ‘सेक्युलर राज्य’ दरअसल एक भ्रामक जुमला है जो भारत की प्राचीन संस्कृति को नकारने का एक साधन मात्र है। “Let us beware and try to survive” इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी बात समाप्त की। बहुसंख्यक धर्म, अल्पसंख्यक पंथ समूह और सेक्युलरिज्म के परिप्रेक्ष्य में संविधान के तुलनात्मक अध्ययन के लिए संविधान सभा में श्री लोकनाथ मिश्रा का सम्पूर्ण भाषण अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है। स्वतन्त्र भारत में सेक्युलरिज्म की उदात्त सैद्धांतिक अवधारणा और उसके अशक्त व्यावहारिक क्रियान्वयन में अंतर इस विडम्बना से उजागर हो जाता है कि श्री मिश्रा संविधान सभा में सेक्युलरिज़्म पर अपना भाषण 3 दिसंबर को इसलिए पूर्ण नहीं कर पाये क्योंकि उस दिन शुक्रवार होने के कारण मुस्लिम बंधुओ की माँग पर उनका भाषण पूर्ण होने के पहले ही सभा भंग कर दी गयी थी।
सन्दर्भ:
[1] CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA – VOLUME VII, Amendment No। 98 ^
[2] CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA – VOLUME III Debate dated 1st May, 1947 ^
[3] Pramati Educational & Cultural Trust versus Union of India 2014 ^
[4] Bramchari Sidheswar Shai and Others vs। State of West Bengal 1995 ^
[5] CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA – VOLUME VII, Amendment No। 591 ^
[6] प्रारूप संविधान का अनुच्छेद 13 अर्थात वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 19 ^
[7] प्रारूप संविधान का अनुच्छेद 19 अर्थात वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 25 ^
_____________
संपादकीय टिप्पणी:
इस उत्तम लेख में लेखक द्वारा प्रयुक्त ‘धर्म’ शब्द को अनेक स्थानों पर ‘पंथ’ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वस्तुत: religion शब्द का अनुवाद धर्म के अर्थ में रूढ़ हो जाने से प्रयोग खटकता नहीं है किंतु यह एक वास्तविकता है कि संविधान के आधिकारिक हिन्दी अनुवाद में सेक्युलर शब्द के लिये ‘पंथ निरपेक्ष’ शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे religion का पंथ अनुवाद स्पष्ट हो जाता है। रामकृष्ण मठ संस्था द्वारा अल्पसंख्यक श्रेणी की माँग को भी इस आलोक में देखा जाना चाहिये। लेखकीय स्वतंत्रता के सम्मान और पाठकों को उनके आलेख के मूल रूप से अवगत कराने हेतु यह टिप्पणी आवश्यक है।
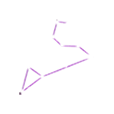







भारत के संविधान के दो प्रावधान कोन से है जो पंथनिरपेक्ष की ओर ले जाते है?