Illusions of pundits theory. क्या मनोवैज्ञानिक पक्षपात से परे होते हैं? क्या उनके मस्तिष्क लोगों और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं? अध्ययनों में इसके रोचक परिणाम मिले हैं।
सनातन बोध : प्रसंस्करण, नये एवं अनुकृत सिद्धांत – 1 , 2, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8, 9 , 10, 11,12, 13, 14 , 15 , 16 से आगे
आधुनिक मनोविज्ञान के सुगम सिद्धांत और उनके सनातन दर्शन में समाहित होने की बात हम पिछले कई लेखांशों से देखते आ रहे हैं। हमने देखा कि कैसे आधुनिक होते हुए भी सारे सिद्धांत सदियों से चले आ रहे दर्शन से निकले हुये प्रतीत होते हैं। इन्हें पढ़ते हुए हमें यह लगने लगता है कि मनोविज्ञान पढ़ने वाले लोगों को जीवन की बहुत गहरी समझ होती होगी। जो मनोविज्ञान का अध्ययन-अध्यापन करते हैं कम-से-कम वे संज्ञानात्मक पक्षपातों से परे होते होंगे। परन्तु क्या सच में ऐसा है?
क्या मनोविज्ञान पढ़ कर समझ भी बढ़ाई जा सकती है?
क्या उसे पढ़कर लोग संज्ञानात्मक पक्षपातों से परे हो जाते हैं?
उनके मस्तिष्क लोगों के और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को भ्रम से परे कर देख पाते हैं?
अध्ययनों में इसके बड़े रोचक परिणाम मिले हैं।
1975 में इस बात को परखने के लिये मिशिगन विश्वविद्यालय के रिचर्ड निज़्बेट और यूजीन बोरगिड़ा ने एक अध्ययन किया। ‘Attribution and the psychology of prediction’ नाम से छपे प्रयोगों पर आधारित इस शोध में उनका निष्कर्ष कुछ यह था कि मनोविज्ञान पढ़ाने का कोई लाभ नहीं! मनोविज्ञान पढने वाले उसे पढ़कर, समझकर उसे परीक्षा में उदाहरणों के साथ लिख कर भी प्राय: कुछ सीख नहीं पाते। वे भी संज्ञानात्मक पक्षपातों के प्रभाव में वैसे ही निर्णय लेते हैं जैसे शेष अनपढ़ लोग।
सिद्धांतों को जान लेने से उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। आधुनिक मनोविज्ञान पढ़कर लोग तथ्यों से सहमत होते हैं, चकित होते हैं। उसे सुनाकर लोगों को अपना ज्ञान दिखा प्रभावित करते हैं। लोगों को उनकी त्रुटियों के कारण भी बता देते हैं अर्थात उन्हें मानव व्यवहार को समझाने का एक यंत्र मिल जाता है परन्तु स्वयं वे वही त्रुटियाँ करते रहते हैं। यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के स्वयं के सम्बंध टूट जाते हैं ! पढ़ने से उनकी स्वयं की समझ परिवर्तित या विकसित नहीं होती।
सिद्धांतों को हम स्वीकार करते हैं, उनसे सहमत होते हैं, परन्तु मात्र सैद्धांतिक रूप से ही। वस्तुत: हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। ऐसी समझ किस काम की? बिना व्यवहार में उतारे विद्या भला किस काम की? हितोपदेश का ज्ञानं भार: क्रियां बिना हो या चाणक्य का –
अनभ्यासे विषं शास्त्रमजीर्णे भोजनं विषम्।
दरिद्रस्य विषं गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम्॥
और बिना आचरण में उतारे ज्ञान के लिये भी तो उन्होंने कहा है –
हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हतश्चाऽज्ञानतो नरः।
हतं निर्नायकं सैन्यं स्त्रियो नष्टा ह्यभर्तृका॥
यह निष्कर्ष रोचक है। परन्तु उससे भी अधिक रोचक बात यह है कि यह निष्कर्ष भी नया नहीं है! (क्योंकि) सनातन दर्शन में तो यह बात तो बार-बार कही गयी है। आधुनिक मनोविज्ञान में illusions of pundits सिद्धांत पढ़ते हुये भला कैसे लग सकता है कि यह कुछ नयी बात है? सिद्धांत ही नहीं, पण्डित शब्द भी! तथा विदुर तो स्पष्ट कह गये हैं – पण्डित वही है जो न केवल विद्या ग्रहण करे बल्कि उसी के अनुरूप अपनी बुद्धि को ढाले और बुद्धि का प्रयोग प्राप्त विद्या के अनुरूप करे।
श्रु प्रज्ञानु यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा। असम्भिन्नायेमयाँद: पण्डिताख्यां लभेत स:॥
जो मान्यतायें हमारे व्यवहार में भीतर गहरी बैठी होती हैं, उन्हें छोड़ना या परिवर्तित करना सरल नहीं होता। शोध का निष्कर्ष – बहेलिया आयेगा, जाल बिछायेगा वाली बोध कथा। भोजपुरी में एक कहावत होती है- “दशा दस बरिस, चलाना चालिस बरिस, सुभाव जिनिगी भर।” अर्थात सब कुछ बदल जाता है, दशा हो या किसी का प्रभाव पर स्वभाव आजीवन वही रह जाता है। इस कहावत में मध्यमान प्रत्यावर्तन से लेकर मनोविज्ञान पढ़ लेने से व्यवहार में परिवर्तन न होने तक की बात आ जाती है!
कबीर के कथनी और करनी से सम्बंधित तो कई दोहे हैं।
कथनी काची होय गई, करनी करी ना सार। स्रोत वक़्त मरि गया, मूरख अनंत अपार।
कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार। कहैं कबीर करनी भली, उतरै भोजन पार।
मनोविज्ञान पढ़कर समझ नहीं बढ़ने से यह निष्कर्ष निकाल लेना कि ‘उसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं’, के स्थान पर मनोवैज्ञानिकों को इन सनातन दर्शनों से उसे अपने आचरण में लाने की बात सीखने की आवश्यकता है।
उक्त शोध का एक निष्कर्ष यह भी था कि जब हम बातों को साधारण सांख्यिकी एवं नियमों की भाँति बताने के स्थान पर व्यक्ति विशेष के उदाहरणों से समझाते हैं तो अधिक समझ में आती हैं। अर्थात मनोविज्ञान पढ़ाने की सटीक विधि व्यक्ति विशेष के ऐसे उदाहरणों से पगी होनी चाहिये जो पढ़ने वालों को विस्मय में डालें। ज्ञान प्राप्ति की यह विधि भी सदियों से प्रचलित रही है, विशेषतया बौद्ध मार्ग में। कितनी ही कहानियाँ हैं जहाँ वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति न होकर एक आश्चर्य चकित कर देने वाली घटना से एक पल में ज्ञान हो गया।
मनोविज्ञान ही नहीं शेष विषयों का भी अध्ययन-अध्यापन ऐसे ही होना चाहिये। मनोविज्ञान में इससे मिलते जुलते कई सिद्धांत हैं यथा तथाकथित विशेषज्ञों को अपने ज्ञानी हो जाने का भ्रम। अति आत्मविश्वास में दोषपूर्ण निर्णय लेने पर ऐसी छद्म विशेषज्ञतायें अधिक घातक सिद्ध होती हैंं। नसीम तालेब कहते हैं कि जो घटनायें घट चुकी हैं उन्हें जब हम देखते हैं तो हमें पूर्व की घटनाओं की समझ होने का भ्रम हो जाता है जो हमारे आत्म विश्वास को बढ़ाता है और हमें लगता है कि हम भविष्य का भी पूर्वानुमान कर सकते हैं। ऐसे कई अध्ययन हैं जिनमें विशेषज्ञों से अच्छे पूर्वानुमान साधारण लोग लगाते हैं। इसका एक कारण यह है कि विशेषज्ञों को अपने ज्ञान का भ्रम हो जाता है, उन्हें लगता है कि उन्हें समझ हो गयी है जिससे वे अति आत्म विश्वास में निर्णय लेते हैं।
भर्तृहरि भला इन अध्ययनों को पढ़ते हुए कैसे मन में नहीं आयेंगे !
अज्ञ: सुखमाराध्य: सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ:। ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि च तं नरं न रंजयति॥
दोष विशेषज्ञों का नहीं है। भविष्य का अनुमान लगाना कठिन है। संसार इतना सरल नहीं है। दोष इसमें है कि विशेषज्ञों को यह भ्रम हो जाता है कि उन्हें समझ हो चली है। उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्हें क्या नहीं पता। पुनः विदुर की उक्ति सटीक बैठती है –
अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः।
अर्थांश्चाकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः।।
प्रिन्स्टन विश्वविद्यालय के प्रो. एमिली प्रोनिन के शोध पत्र The Bias Blind Spot: Perceptions of Bias in Self Versus Others में वर्णित पक्षपात अंध बिंदु (bias blind spot) सिद्धांत कहता है कि हमें दूसरों के पक्षपात अधिक दिखाई देते हैं, अपने नहीं। इसी क्रम में मायावी श्रेष्ठता (Illusory superiority) का सिद्धांत भी आता है जिसके अनुसार हम अपने गुणों को अधिक करके आँकते हैं। इसे औसत से अधिक प्रभाव (Above-average effect) भी कहते हैं क्योंकि सर्वेक्षणों में प्राय: सभी लोग अपने को औसत से उत्तम मानते हैं। आश्चर्य यह है कि यदि सभी औसत से अच्छे होते हैं तो औसत बनता कैसे है ! आश्चर्य है कि सबको यही लगता है कि वह शेष लोगों की तरह नहीं है। युधिष्ठिर के ‘किम् आश्चर्यम्’ की भाँँति। दूसरों के दोष देख अपनी नहीं देख पाने वालों के लिये कबीरदास का ‘बुरा जो देखन मैं चला’ से लेकर विदुर के मूढ़ तक अनेकों संदर्भ हैं –
परं क्षिपति दोषेण वर्त्तमानः स्वयं तथा। यश्च क्रुध्यत्यनीशानः स च मूढतमो नरः॥
(क्रमश:)
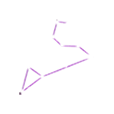







कंप्सूयूटर आदि किसी डिवाइस के RAM/ROM में चनाओं का असीमित भंडार एकत्र हो जाने से उसका व्यवहार नहीं बदल सकता। मतलब यदि डिवाइस के साॅफ्टवेयर में निर्माणगत त्रुटि है तो वह असीमित ज्ञान पूर्ण सूचनाऐं उपलब्ध होने पर भी यंत्र त्रुटि करेगा है। इससे मुक्ति का उपाय तो केवल साॅफ्टवेयर का उप्युक्त अपडेट वर्जन इंस्टाल करना ही है। ठीक ऐसा ही मानव व्यवहार के लिए भी है।