Emotional intelligence भावात्मक प्रज्ञा या संवेगात्मक बुद्धि विगत वर्षों में मनोविज्ञान तथा प्रबंधन में एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत बन कर उभरी है। इसका अर्थ स्वयं तथा दूसरों की भावनाओं का समुचित संज्ञान रखने, उन्हें समुचित रूप से व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है, अर्थात भावनाओं का प्रबंधन।
जिन व्यक्तियों में स्वयं तथा दूसरों की भावनाओं तथा संवेगों का अभिज्ञान कर उसके अनुरूप सोचने तथा व्यवहार करने की क्षमता होती है, वे भावात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान होते हैं। भावात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों से उचित संवाद भी कर पाते हैं जिससे उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। अनेक विचारकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने जीवन में सफलता के लिए इसे बौद्धिक स्तर के मापाङ्क बुद्धि लब्धि (Intelligence Quotient) से भी अधिक महत्त्वपूर्ण माना है। सफलता के लिए अधिक बुद्धि लब्धि के साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भावनात्मक रूप से अल्प-बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय लेते समय क्रोध, प्रसन्नता, ईर्ष्या इत्यादि से प्रभावित हो अनुचित निर्णय ले लेते हैं।
पश्चिमी मनोविज्ञान में भावात्मक बुद्धि एक नवीन सिद्धांत है जिसे परिभाषित करने के प्रारूप भी नए हैं, जिनमें सामाजिक वातावरण के अनुरूप व्यक्ति की प्रतिक्रिया, व्यवहार, आत्म वर्णन तथा व्यक्ति के कौशल को विशेषताओं की सारणी से मापा जाता है। अन्य अध्ययनों में तंत्रिका तंत्र में भावनात्मक बुद्धि के कारणों को चिन्हित करने के भी प्रयास किए गए हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सामान्यतया तीन कौशलों की प्रमुखता है – भावात्मक अभिज्ञता (emotional awareness, self-awareness) अर्थात स्वयं की भावनाओं का संज्ञान, उस संज्ञान का विचार और समस्याओं के हल में समुचित प्रयोग और भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता।
भावना अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति मनोभाव। बहुधा ये मनोभाव अनजाने में बिना सोची समझी अवस्था में होते हैं परंतु हमारे तार्किक निर्णय की क्षमता को प्रभावित करते हैं। साथ ही इन भावनाओं को समझना तथा उनका वर्गीकरण करना भी अत्यंत कठिन कार्य है। जहाँ कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार भावात्मक बुद्धि अभ्यास से सीखी जा सकती है वहीं अन्य के अनुसार यह एक जन्मजात गुण है। पश्चिमी मनोविज्ञान तथा प्रबंधन में इस लोकप्रिय सिद्धांत का जन्म पीटर सलोवे और जॉन मेयर के वर्ष १९९० ग्रे. में प्रकाशित एक आलेख से माना जा सकता है। वर्ष १९८५ के पहले इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। वर्ष १९९५ में डेनियल गोलमैन की पुस्तक emotional intelligence से इसे विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली। जिसके पश्चात मनोविज्ञान के बाहर शिक्षा और प्रबंधन में भी इस विषय ने अपना स्थान बनाया। मनोवैज्ञानिकों के लिए यह बुद्धिमत्ता के परे दिखने वाली सफलता के कारणों का वर्णन करती है। इससे पहले पश्चिमी मनोवैज्ञानिक बुद्धि (intelligence) के इस पक्ष को नहीं जानते थे।
भावात्मक बुद्धि के उदाहरण सरल हैं :
-
दूसरों की अवस्था समझना और यह समझना कि दूसरे जो कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं।
-
और कोई भी क्षणिक प्रतिक्रिया देने से पहले वस्तुस्थिति को समझना।
-
हमारे स्वयं की भावनाओं (संवेगों) को समझने तथा नियंत्रित करने की योग्यता।
-
साथ साथ दूसरों की भावनाओं एवं संवेगों को समझना।
दूसरों की भावनाओं एवं संवेगों को समझते हुये उन्हें सम्मान देना भी महत्वपूर्ण हैं जिससे निर्णय लेते समय हम उनसे प्रभावित न हों । विगत वर्षों में भावात्मक बुद्धि में सुधार के अनेक कार्यक्रम विकसित किए गए हैं जिनमें मुख्य रूप से ध्यान से सुनना, दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करना तथा मनन करने के क्रियाकलाप (listen, empathize, reflect) प्रमुख हैं।
अर्थात ऐसी बुद्धि का विकास जिसमें भावनाओं एवं संवेगों का कोई स्थान नहीं हो। किसी के क्रोध, दुःख इत्यादि का उचित संज्ञान कर व्यवहार करना तथा निर्णय लेना, इसे ‘समबुद्धि योग्यता’ भी कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समबुद्धि की अवधारणा व्यक्तियों की प्रबंधन प्रणाली को एक नई दिशा प्रदान करती है तथा व्यक्ति एवं समाज को सृजनात्मक तथा सकारात्मक बनाती है। नेतृत्व के पदों पर व्यक्तियों में इन गुणों की प्रमुखता विशेष रूप से चिह्नाङ्कित की गयी है।
भावात्मक बुद्धिमत्ता पर सबसे प्रमुख पुस्तकों तथा अध्ययनों को समझने के पश्चात उसका सार ‘स्थितप्रज्ञ व्यक्ति’ की परिभाषा ही प्रतीत होता है तथा उसके लिए लिए विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम सनातन आत्मबोध तथा सम-दृष्टि मात्र विकसित करने का कार्य करते हैं। उपनिषदों एवं अन्य वैदिक वाङ्मय तथा अन्य ग्रंथों में मानव मन, इंद्रियों तथा उसके नियंत्रण का महत्त्व के अनेक संदर्भ उपलब्ध हैं। गीता के द्वितीय अध्याय में संवेगात्मक बुद्धि के इन अध्ययनों की विस्तृत व्याख्या मिलती है।
सार तो इस श्लोक में ही मिलता प्रतीत होता है –
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥
और स्थितप्रज्ञ तो मानों परिभाषा ही है emotional intelligence का –
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥
यदि संवेगों के चिंतन से दूर रहने की बात हो तो –
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात् संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥
प्रबंधन या नेतृत्व कैसा हो? का उत्तर यदि भावनाओं के परे सम-दृष्टि हो तो –
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥
आत्म बोध (self-awareness) तो सनातन ग्रंथों का मूल ही है और सहानुभूति की बात हो तो यह देखें –
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥
इस दर्शन से उत्कृष्ट और क्या सिद्धांत हो सकता है।
आश्चर्य नहीं कि इस नए सिद्धांत के सन्दर्भ में वर्ष २०१० में भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर द्वारा कराए गए एक अध्ययन में योग को भी भावात्मक बुद्धिमत्ता में वृद्धि का उपाय पाया गया।
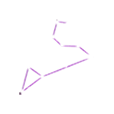

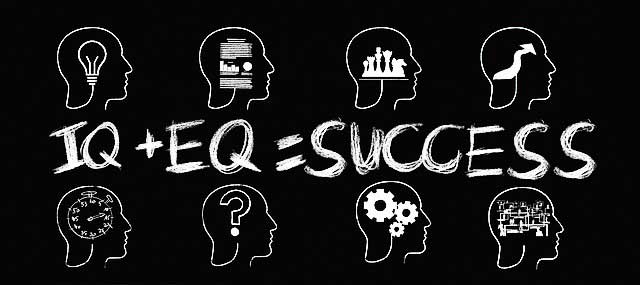






Iq+eq=success , it’s true sir assisment of teaching or developmental assisment in human.